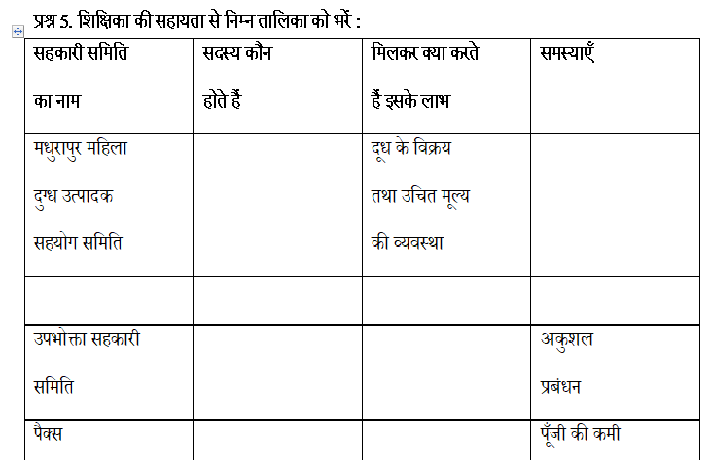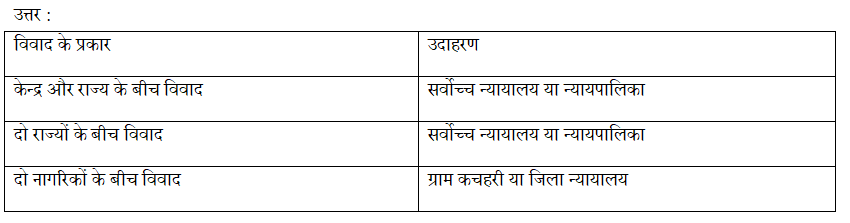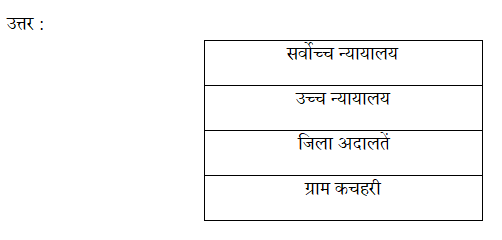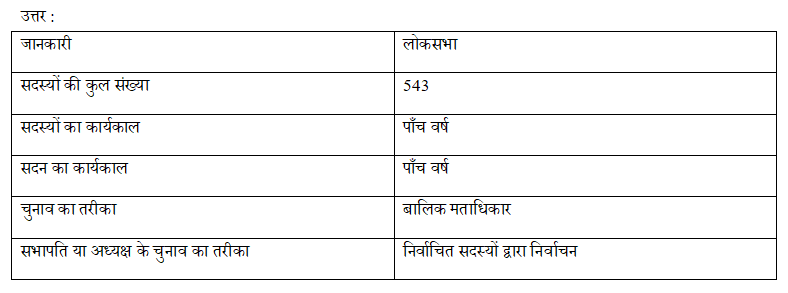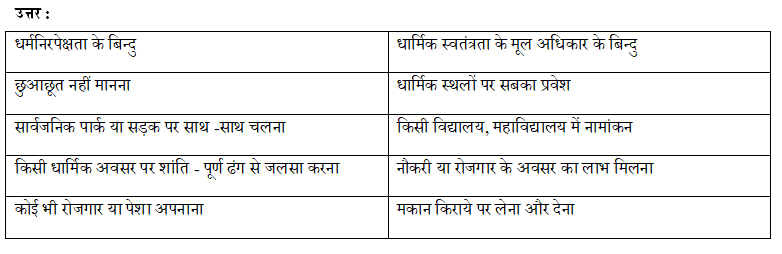इस पोस्ट में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल के पाठ इकाई 1 (क) भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के अर्थ को पढ़ेंगे। Bhumi Mrida Evam Jal Sansadhan Notes, bihar board class 8th social science solutions, Bhumi Mrida Evam Jal Sansadhan mcq Questions, bhumi mrida evam jal sansadhan question answer, bhumi mrida evam jal sansadhan important questions, class 8 bihar board geography solutions, Bhumi Mrida Evam Jal Sansadhan Notes, Bhumi Mrida Evam Jal Sansadhan Notes

इकाई 1 (क) भूमि, मृदा एवं जल संसाधन
पाठ के अन्दर आए प्रश्न और उत्तर
प्रश्न 1. भूमि के विविध उपयोग की चर्चा कीजिए ।
उत्तर – भूमि का प्रमुख उपयोग तो कृषि कार्य में है, जिससे सबको अन्न, सब्जी, फल- मूल प्राप्त होते हैं। वन और विभिन्न प्रकार के वृक्ष भूमि पर ही उगते या उगाये जाते हैं। सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग — भूमि पर ही बनाये जाते हैं। हवाई जहाज उड़ते तो हवा में हैं, लेकिन हवाई अड्डा भूमि पर ही होता है। यही हाल समुद्री जहाजों का है, जो चलते तो समुद्र के पानी पर हैं, लेकिन इनके बन्दरगाह भूमि पर ही बनते हैं । कल-कारखानों का निर्माण भी भूमि पर ही होता है। आवास के लिए मकान भी भूमि पर ही बनाये जाते हैं। गाँव हो या बाजार या कस्बा चाहे शहर, नगर या महानगर — ये सभी भूमि पर ही बसते हैं। तालाब, नहर, कुआँ आदि भूमि पर ही बनते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जीव- आदमी हो या पशु-पक्षी, सभी काजीवन जमीन सेजुड़ा है।
प्रश्न 2. नवी मुंबई का विकास कहाँ और कैसे किया गया ?
उत्तर – मुंबई से सटे एक बड़ा क्षेत्र दलदली था । प्रयासपूर्वक उसे सुखाकर ठोस भूमि बनाई गई । उसी भूमि पर नवी मुंबई का विकास हुआ है । उस भूमि को ठोस बनाने के लिए मानव श्रम का उपयोग कर पत्थर और मिट्टी से भरा गया, तब जाकर ठोस भूमि प्राप्त हुई ।
प्रश्न 3. राजस्थान के गंगा नगर क्षेत्र के विषय में आप क्या जानते हैं? उसे उपजाऊ कैसे बनाया गया ?
उत्तर – राजस्थान राज्य का गंगा नगर क्षेत्र पहले बलुई और अनुर्वर था। नदी पर बाँध बनाकर उस क्षेत्र में नहर को विकसित किया गया। इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त. हो गई । फल हुआ कि वह क्षेत्र काफी उपजाऊ हो गया। आज गंगा नगर क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र में गिना जाने लगा है।
प्रश्न 4. मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। क्यों? (पृष्ठ 22)
उत्तर – यह सही है कि मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। लेकिन सभी मिट्टी मृदा नहीं है । धरातल के कुल सेमी ऊपरी भाग को ही मृदा कहा जाता है, जितनी गहराई तक कृषि कार्य होता है । इस अर्थ में सभी मृदा मिट्टी तो है, लेकिन सभी मिट्टी मृदा
नहीं है। मृदा के नीचे के भाग को मिट्टी कहते हैं ।
प्रश्न 5. ह्यूमस क्या है? (पृष्ठ 22)
उत्तर – पेड़-पौधों के पत्ते, मृत जन्तुओं के शरीर, सड़े-गले पदार्थ और उनके अवशेष मृदा में मिलकर ह्यूमस बनाते हैं । ह्यूमस खासतौर पर मिट्टी के सबसे ऊपर के स्तर में पाये जाते हैं। इससे मृदा उपजाऊ बनती है।
प्रश्न 6. आपके आस-पास में मिट्टी का क्या उपयोग होता है ? (पृष्ठ 23)
उत्तर – मेरे आस-पास में मिट्टी के अनेक उपयोग हैं । जैसे :
(क) घर की दीवार बनाना, (ख) छप्पर के लिये खपड़ा तथा नरिया बनाना (ग) मिट्टी के बरतन : जैसे घड़ा, सुराही, हांड़ी, ढकना और ढकनी, (घ) ईंटे बनान तथा (ङ) बच्चों के लिए खिलौने बनाना ।
प्रश्न 7. मृदा अपरदन क्या है? (पृष्ठ 26)
उत्तर –आँधी, वर्षा, बाढ़ आदि प्राकृतिक कारणों से मृदा का स्थान परिवर्तन मृत् अपरदन कहलाता है। कभी-कभी मानवीय कारक भी कारण बनते हैं ।’
प्रश्न 8. विभिन्न महासागरों में जल का वितरण दर्शाइए । (पृष्ठ 27)
उत्तर – विभिन्न महासागरों का जल वितरण निम्नांकित है :
(i) प्रशांत महासागर 49.9%
(ii) अटलांटिक महासागर 25.7%
(iii) हिन्द महासागर 20.5%
(iv) आर्कटिक महासागर 3.9%.
प्रश्न 9. जलचक्र क्या है ?
उत्तर – महासागर का जल वाष्प बनकर बादल बनता है। कुछ वाष्प वायु में भ मिल जाता है। बादल वर्षा कर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं और कुछ वाष्प पहाड़ों प बर्फ बन जाते हैं । बर्षा जल तथा बर्फ से बना जल नदियों में जाते हैं और नदियों वे माध्यम से पुनः समुद्र में पहुँच जाते हैं । यह चक्र सदैव चलते रहता है । इसी को जलचक्र (water cycle) कहते हैं ।
अभ्यास : प्रश्न तथा उनके उत्तर
1. बहुवैकल्पिक प्रश्न :
सही विकल्प को चुनें
1. पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत है ? (क) 71 (ख) 29 (ग) 41 (घ) 46
2. विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है ?
(क) पहाड़ों पर
(ख) पठारों पर
(ग) मैदानों में
(घ) मरुस्थल में
3. भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं ?
(क) 9
(ख) 7
(ग) 5
(घ) 3
4. मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं ?
(क) 2
(ख) 3
(ग) 4
(घ) 7
5. समोच्चरेखीय खेती करना किसका उपाय है ?
(क) जल प्रदूषण को रोकने का
(ख) मृदा अपरदन को रोकने का
(ग) जल संकट को दूर करने का
(घ) भूमि की उर्वरता घटाने का
6. रासायनिक दृष्टि से जल किसका उपाय है ?
(क) हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का
(ख) ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का
(ग) हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का
(घ) ऑक्सीजन एवं कार्बन का
7. इनमें कौन एक महासागर नहीं है ?
(क) अंटार्कटिक
(ख) आर्कटिक
(ग) हिन्द
(घ) प्रशांत
उत्तर : 1. (ख), 2. (ग), 4. (ग), 5. (ग), 6. (ख), 7.(ग), 8. (क)
2. खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें ।
1. मृदा में जीवों के सड़े-गले अवशेषों को ……………… कहा जाता है ।
2. दक्कन क्षेत्र में ……………….. मृदा पाई जाती है ।
3. लैटेराइट मृदा का निर्माण ……………… प्रक्रिया से होता है ।
4. भूमि एक ……………….. संसाधन है ।
5. महासागरों में जल का ……………भाग पाया जाता है ।
उत्तर : 1. ह्यूमस, 2. लाल-पीली, 3. निक्षालन, 4. महत्वपूर्ण, 5. 97.3 प्रतिशत ।
(अधिकतम 50 शब्दों में)
Bhumi Mrida Evam Jal Sansadhan Notes
III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें ।
प्रश्न 1. भूमि उपयोग से क्या समझते हैं?
उत्तर—भूमि के अनेक उपयोग हैं। भूमि पर कृषि कार्य होते हैं, जिससे हमें अन्न और सब्जियाँ प्राप्त होती हैं। बाग-बगीचे भूमि पर ही लगाए जाते हैं, जिनसे हमें फल मिलते हैं। मकान, गाँव-नगर, तालाब – नहर, कुआँ और चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइप लाइन मार्ग, कारखाने, विद्यालय और खेलों के मैदान भूमि पर ही बनते हैं ।
प्रश्न 2. मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए ।
उत्तर – मृदा निर्माण में स्थान विशेष में उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊँचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। सर्वप्रथम चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कण और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। लाखों-लाख वर्षो बाद चट्टानी टुकड़े भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण आदि के फलस्वरूप महीन कणों में बदल जाते हैं, जिनसे मृदा का निर्माण हो जाता है।
प्रश्न 3. भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए।
उत्तर- भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं :
(i) वन क्षेत्र की भूमि, (ii) कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, (iii) परती भूमि, (iv) स्थायी चारागाह और बंजर भूमि, (v) शुद्ध बोयी गई भूमि ।
प्रश्न 4. भूमि उपयोग के पाँच वर्गों का उल्लेख कीजिए ।
उत्तर— (i) बंजर एवं व्यर्थ भूमि, (ii) सड़क, मकान और उद्योगों में प्रयुक्त भूमि, (iii) चालू परती भूमि, (iv) स्थाई चारागाह भूमि, (v) कृषि कार्य में लगी भूमि तथा (vi) खनिज संसाधनों की भूमि ।
IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें । (अधिकतम 200 शब्दों में)
प्रश्न 1. भूमि उपयोग क्या है ? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।
उत्तर—कृषि कार्य करना, बाग-बगीचे लगाना, गाँव और शहर बसाना, तालाब, नहर और कुएँ खुदवाना, सड़क, रेल, पाइप लाईन, कारखानें आदि लगाना कार्य को भूमि उपयोग कहते हैं ।
(i) वन क्षेत्र की भूमि – वन भूमि पर ही उगते हैं और प्राकृतिक रूप से उगते, बढ़ते और फलते-फूलते हैं । जिस क्षेत्र की भूमि पर जितने ही अधिक वन होते हैं, वहाँ की जलवायु उतनी ही अनुकूल होती है ।
(ii) कृषि कार्य में उपयुक्त भूमि- कृषि कार्य भूमि पर ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अन्न या सब्जी सभी भूमि पर उग सकते हैं । कहीं की भूमि चावल के लिए उपयुक्त है तो कहीं की गेहूँ के लिए । अरहर, मसूर, मूँग, उड़द आदि सभी सर्वत्र नहीं उपज पाते। गन्ना और कपास के लिए भूमि अलग प्रकार की होती है ।
(iii) परती भूमि — गाँवों में कुछ-न-कुछ परती भूमि भी होती है। शहरों में परती के स्थान पर बड़े-बड़े मैदान होते हैं। गाँव की परती भूमि चारागाह तथा बच्चों के खेलने- कूदने के काम आती है ।
(iv) अन्य कृषि – अयोग्य भूमि – कुछ गाँवों में स्थायी चारागाह होता है, जहाँ गाँव के लोग गाय-भैंस तथा भेड़-बकरी चराते हैं । इसी कोटि में कुछ बंजर भूमि भी हैं, जिनमें चार-पाँच वर्षों पर कभी-कभार एक फसल उगाई जा सकती है ।
प्रश्न 2. मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर – मृदा निर्माण में स्थानीय मौलिक चट्टान, उस क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊँचाई, वहाँ की ढाल तथा वर्षा के परिमाण पर निर्भर है । सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया सदा चलती रहती है। हजारों-लाखों वर्षों के बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक और जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो ‘मृदा’ कहलाता है। सामान्यतः एक से चार सेंटीमीटर ऊपरी मोटी तह को मृदा कहते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सभी मृदा मिट्टी है, किन्तु सभी मिट्टी मृदा नहीं है। मृदा केवल उसी भाग को कहते हैं, जिनमें कृषि कार्य होते हैं। मृदा के बनने में हजारों-हजार वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण को दो भागों में बाँटा गया है। (i) जैविक, और रासायनिक ऋतुक्षरण से तथा (ii) भौतिक ऋतुक्षरण
से ।
(i) जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण— पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं, मानवीय प्रक्रियाओं तथा वर्षा जल के बहने वाली प्रक्रिया से चट्टानें टूटती, घिसती गलती रहने वाली प्रक्रियाएँ रासायनिक ऋतुक्षरण कहलाती हैं ।
(ii) भौतिक ऋतुक्षरण- तापमान का बढ़ना – घटना, तुषार की क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने-सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है ।
मिट्टी के मुख्यतः चार स्तर होते हैं । नीचे से ऊपर क्रमशः मौलिक चट्टान, ऋतुक्षरित कण, बालू एवं पंक तथा ह्यूमस । ऊपर का ह्यूमस वाला भाग ही मृदा हैं ।
प्रश्न 3. मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए ।
उत्तर—मृदा अपरदन के तीन कारक हैं। (i) वर्षा जल, (ii) पवन तथा (iii) नदियाँ । वर्षा जल अपने साथ मृदा को बहा ले जाता है। दूसरा कारक तेज पवन मृदा को उड़ा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देते हैं। नदियों में बाढ़ का पानी जब धीरे- धीरे नदियों में पहुँचता है, तो नदियों के तट को काटकर मिट्टी को बहा ले जाता है । ( हालाँकि बाढ़ वाली नदी अपने किनारों पर नई उपजाऊ मिट्टी फैला भी देती हैं। गंगा- ब्रह्मपुत्र के मैदान इन नदियों द्वारा बाढ़ में लाई मिट्टी द्वारा ही बने हैं ।)
।
पेड़-पौधे, झाड़ियों तथा घासों की जड़ें मृदा को पकड़े रहती हैं, जिससे वर्षा जल का बहाव या बूँदों की मार से मृदा कटने और बहने नहीं पाती । वास्तव में पेड़-पौधों को जड़ सहित काटने, उखाड़ने तथा घासों को छील देने के कारण वहाँ की भूमि ढीली पड़ जाती है। ऐसी ही मृदा बहकर या उड़कर अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है । अतः यदि हम मृदा अपरदन को रोकना चाहते हैं तो पेड़ों, झाड़ियों और घासों को बिल्कुल न काटें और न उखाड़े ।
इसके अलावे पशुचारण, आकस्मिक तेज़ वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति भी मृदा अपरदन के कारक बनते हैं । अतः इन बातों की रोकथाम का उपाय करने से मृदा अपरदन नहीं होगा ।
मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं :
(i) पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्चरेखीयं खेतों की जुलाई की जाय ।
(ii) पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण किया जाय ।
(iii) ऐसे ढलानों पर घास छिलने या पशुचारण पर रोक लगे ।
(iv) बंजर भूमि पर घास और पेड़ लगाए जाएँ ।
(v) फसल चक्र तकनीक को निश्चय ही अपनाया जाय ।
(vi) खेती के वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएँ ।
(vii) रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो तथा जैविक खाद का उपयोग अधिक से-अधिक हो ।
प्रश्न 4. जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसको दूर करने के उपारों का वर्णन कीजिए ।
उत्तर— जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं । जैसे घरेलू कूड़ा-कर्कट को कुओं के निकट या नदियों के किनारे फेंकना। औद्योगिक कारखानों से निकले तरल अपशिष्ट पदार्थो को नदियों में गिराने से उस नदी का जल उपयोग के काबिल नहीं रहता । नगरों के सीवर तथा नालो का जल नदियों में गिरा दिया जाता है। यह प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है । यह जल प्रदूषण का एक अति जिम्मेदार पहलू है। नदियाँ परिवहन का भी कार्य करती हैं। नांविक और यात्री उसी नदी में मल-मूत्र का त्याग करते हैं । इससे भी जल प्रदूषित होता है। गाँवों में कुओं के निकट पखानों का शौक पीट रहने से उसका दूषित जल भौम जल में मिलते रहता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है ।
जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं
(i) वर्षा जल संग्रहण की तकनीक अपनाना ।
(ii) छत का वर्षा जल संग्रहित करना ।
(iii) जल स्रोतों के निकट गंदगी नहीं फैलाना ।
(iv) नदी तटों पर कूड़ा-कर्कट नहीं फेंका जाय ।
(v) नगर के सीवर तथा नालों के जल को संसाधित करके ही नदियों में गिराना ।
(vi) कारखाने का अपशिष्ट जल भी संसाधित कर नदियों में गिराया जाय । लोगों को चाहिए कि वे स्वयं उपरोक्त विधियाँ अपनावें तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने को प्रेरित करें ।
प्रश्न 5. जल संकट क्या है ? जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का विवरण दीजिए ।
उत्तर – जल प्राप्ति में दिक्कत या जल की कमी को जल संकट कहते हैं । पृथ्वी पर पीने योग्य जल की भारी कमी है। यह मात्र कुल जल का मात्र 1% से भी कम है । जितना जल है उसका भी असामान वितरण है। देश में कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ के लोग कई किलोमीटर दूर से जल लाते हैं । इन्हीं सब बातों को मिला-जुलाकर जल संकट कहा जाता है ।
जल संकट के कारक निम्नलिखित हैं :
जनसंख्या में अपार वृद्धि होती जा रही है। 20वीं सदी के चौथे दशक में जहाँ अविभाजित भारत की जनसंख्या जहाँ 35 करोड़ थी वहीं आज पाकिस्तान और बंगलादेश को अलग हो जाने के बावजूद भारत की जनसंख्या सवा अरब हो गई है। अब इतने लोगों को जल तो चाहिए ही चाहिए। नगरों बहुमजली इमारतें बनती जा रही हैं। सभी मंजिलों पर पानी पहुँचाने के लिए बोरिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस कारण जल स्तर नीचे भागता जा रहा है। नगरों में जल संकट का यह भी एक कारण है। प्रदूषण के कारण भी जल उपयोग योग्य नहीं रह पाता ।
जल संकट से बचने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी। इसके लिए प्राकृतिक तथा कृत्रिम उपायों का सहारा लेना होगा । नगरों में भू-जल के परिपूर्णन का उपाय करना होगा। जमीन में पाइप धँसाकर वर्षा जल को उस पाइप के सहारे भूमि के अन्दर पहुँचाना पड़ेगा। इससे जल स्तर अपनी समान सीमा में बना रहेगा । जल प्रदूषण नहीं होने पावे, इस पर भी ध्यान देना होगा ।
प्रश्न 6. भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
उत्तर—भारत में निम्नलिखित मृदाएँ पाई जाती हैं :
(i) जलोढ़ मृदा – जलोढ़ मृदा बाढ़ वाले मैदानी भागों में मिलती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों ने उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में जलोढ़ मृदा को फैला रखा है । इसके अलावा राजस्थान तथा गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
(ii) काली मृदा – जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है काली मृदा का रंग काला होता है । ऐसी मृदा में एल्युमीनियम एवं लौह यौगिक पाए जाते हैं । यह मृदा कपास की उपज के लिए काफी उपयुक्त होती है । इस कारण इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। खासतौर पर ऐसी मृदा दक्कन पठार के लावा प्रदेशों में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में भी यह पाई जाती है ।
(iii) लाल एवं पीली मृदा- लाल एवं पीली मृदा का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में ग्रेनाइट तथा नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के टूटने से हुआ है। खासकर ऐसी मृदा वहाँ पाई जाती है, जहाँ 100 सेमी से कम वर्षा होती है । इसमें लोहा का अंश अधिक मात्रा में रहता है, इसी कारण इसका रंग लाल रहता है । जलयोजन के बाद इसका रंग पीला हो जाता है। ऐसी मृदा का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटानागपुर और मेघालय में है ।
(iv) लैटराइट मृदा – लैटराइट मृदा का विकास उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। खासकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लैटराइट मृदा पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अधिक तापमान के कारण अपघटक वैक्टेरिया नष्ट हो गए रहते हैं । अपक्षय के कारण यह मृदा कठोर हो जाती है । इसमें लोहा और एल्युमीनियम के आक्साइड मिले होते हैं, जिससे इसका रंग लाल होता है। यदि तकनीक का सहारा लिया जाय तो चाय, कहवा और काजू उपजाने के लिए यह मृदा उपयुक्त है ।
(v) मरुस्थलीय मृदा – ऐसी मृदा बलूई किस्म की, ह्यूमस रहित, हल्का लाल या भूरे रंग की होती है। इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा, दक्षिणी पंजाब तक में है। सिंचाई और उर्वरकों की व्यवस्था से ऐसी मृदा में कपास, धान, गेहूँ, तेलहन आदि की अच्छी उपज हो पाती है ।
(vi) पर्वतीय मृदा – अपने नाम के अनुरूप पर्वतीय मृदा पर्वतों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा जटिल और विविधता वाली होती है। ऊँचे भागों में पाई जाने वाली मृदा मोटे कणों वाली है । जहाँ अधिक वर्षा होती हैं, वहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं सदाबहार वन निचले भागों में होते हैं। नदी घाटियों, नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में पर्वतीय मृदा उपजाऊ होती है, जहाँ धान, आलू आदि उपजाए जाते हैं और फलों के बगान लगाए जाते हैं ।
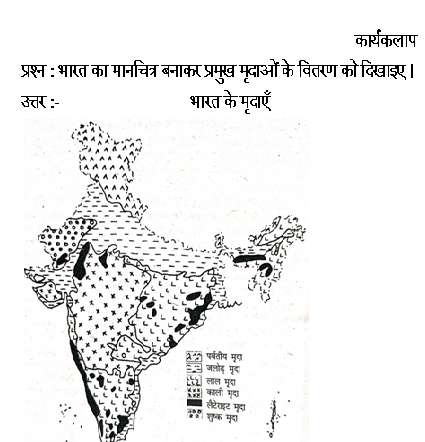
Bhumi Mrida Evam Jal Sansadhan Notes
Read more- Click here
You Tube – Click here